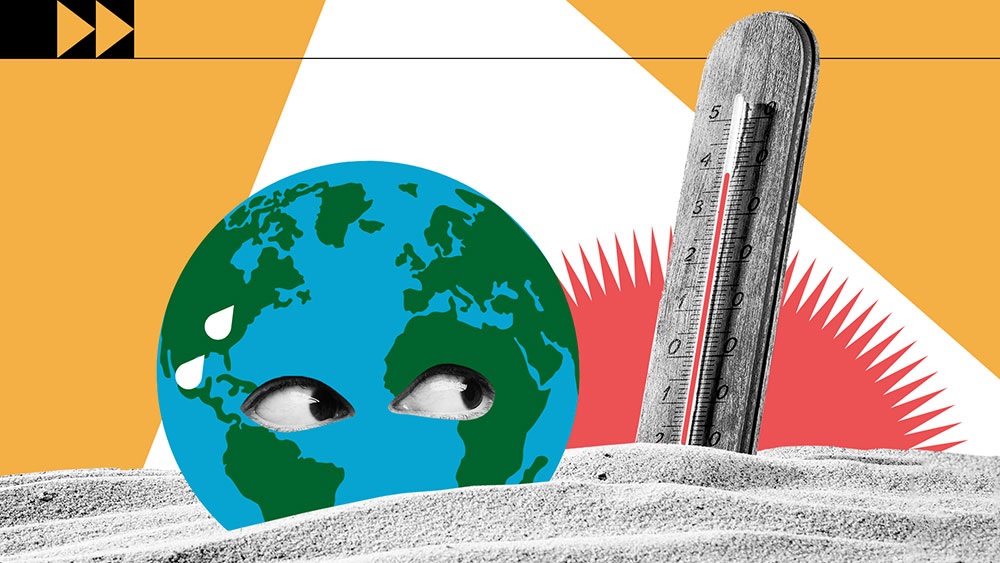सब जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन की मौजूदा त्रासदी की वजह धरती पर बसे इंसानों की हवस पर आधारित जीवन-पद्धति है, लेकिन कोई इसे रोकना, बदलना नहीं चाहता। वैश्विक स्तर पर भी ठीक यही हालत है और तरह-तरह के जमावडों के बावजूद कोई देश संयम नहीं बरतना चाहता। क्या होते हैं, इसके नतीजे?
दुबई में हुए 28वें ‘जलवायु परिवर्तन सम्मेलन’ (कॉप28) में ‘संयुक्त राष्ट्र संघ’ के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने चेतावनी दी थी कि दुनिया तबाही की कगार पर है और यह सम्मेलन हमें आखिरी मौका दे रहा है। इस सम्मेलन में दुनिया के 200 देश डीजल, पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल से दूरी बनाने पर सहमत दिखाई दिये। जीवाश्म ईंधन ‘ग्लोबल वार्मिंग’ का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। यदि इस पर निर्भरता धीरे-धीरे घटायी जा सके तो जलवायु को नियंत्रित किया जा सकता है।
इससे पहले वर्ष 2015 में ‘संयुक्त राष्ट्र संघ’ द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों व सामूहिक प्रगति पर नजर रखने के लिए पेरिस में भी 200 से अधिक देशों का सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन के समझौते के अनुसार वैश्विक तापमान वृद्धि को ‘पूर्व औद्योगिक काल’ (1850-1900) के स्तर के मुकाबले 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है, लेकिन महसूस किया गया कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आवश्यक निधि अपर्याप्त है।
पिछले सम्मेलनों में संयुक्त-अरब-अमीरात की तरफ से इसका विरोध हुआ था। उसका कहना था कि जब तक नवीकरणीय ऊर्जा के पर्याप्त स्रोत उपलब्ध नहीं हो जाते, तब तक जीवाश्म ईंधन पर बंदिशें लगाना उचित नहीं है क्योंकि दुनिया की 80 फ़ीसदी ऊर्जा ज़रूरतें इसी से पूरी हो रही है। दूसरी तरफ वे यह भी कह रहे हैं कि जीवाश्म ईंधन से दूर रहने के लिए वे भी सहमत हैं। इसके साथ ही 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा गया है।
40 से अधिक देशों और 20 संगठनों के मंत्रियों, नीति निर्माताओं, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने एक वार्ता करके कहा है कि वे वैश्विक स्तर पर स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना बढ़कर 11 हजार गीगावॉट करने और इस समय सीमा में वार्षिक ऊर्जा दक्षता सुधार को दोगुना करने के लक्ष्य प्राप्त करने पर सहमत हैं, लेकिन इसे हासिल करने के लिए 4.5 खरब डालर की आवश्यकता है।
वर्ष 2009 में कोपनहेगन में हुई जलवायु वार्ता में प्रस्तावित “हरित जलवायु निधि“ में अमीर देशों ने 2020 तक, हर साल विकासशील देशों को 100 अरब डॉलर की मदद करने का संकल्प लिया था, लेकिन किसी भी साल वे इस राशि को नहीं जुटा सके। इन देशों ने 2013 में 52.5 अरब डॉलर जुटाए थे जो 2015 में घटकर 44.6 अरब डॉलर हो गए थे। 2019 में उनकी तरफ से 80.4 अरब डॉलर का फंड संग्रह किया गया था जो 2020 में बढ़कर 83.3 अरब डालर हो गया था। अब तो 100 अरब डॉलर से भी अधिक की आवश्यकता महसूस की जा रही है। ऐसे में 2030 तक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखने के प्रयासों को झटका लग सकता है।
एक अनुमान के मुताबिक दुनियां के 55 देशों को बीते दो दशक में जलवायु परिवर्तन संबंधी घटनाओं से 525 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। 2030 तक यह बढ़कर 580 अरब डालर पहुंच जाएगा। वहीं अगर अकेले अमेरिका से उसके उत्सर्जन प्रभाव की कीमत वसूली जाए तो यह 1900 अरब डॉलर होती है। विकासशील देशों का सवाल है कि क्या अमेरिका इस कीमत को चुकाएगा? अगर नहीं तो फिर किसी दूसरे देश से कैसे कह सकते हैं कि वह विकास न करे। इस संदेश से ऐसा लगता है कि सभी देश अमेरिका की राह पर हैं और आधुनिक जीवन शैली व विकास के मायने जलवायु परिवर्तन ही है।
जीवाश्म ईंधन के उपयोग का आखिरी पन्ना 28वें जलवायु सम्मेलन में नहीं पलटा जा सकता है, लेकिन जीवाश्म ईंधन के अंत की शुरुआत यहां से की जा सकती है। इसके लिए कोयला से बिजली बनाने वाले देश, जैसे – भारत और चीन से भी अपेक्षा की जा रही है कि वे चरणबद्ध तरीके से कोयले के उपयोग में कमी करें, हालांकि भारत विकसित देश बनने तक कोयले पर कितना नियंत्रण कर सकेगा, यह तो समय ही बताएगा। मजबूत विकल्प के अभाव में जीवाश्म ईंधन और कोयले पर निर्भरता को चरणबद्ध तरीके से कम करने की तैयारी अभी भी नगण्य है। दूसरी ओर विकल्प के तौर पर परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करें तो रेडियोएक्टिव कचरे को लेकर खतरे की आशंका जताई जाती रही है।
विकासशील देश विकसित देशों पर आरोप लगा रहे हैं कि वे अपना योगदान देने की बजाय भारत, ब्राजील, चीन जैसे देशों पर दबाव बना रहे हैं कि वे विकास के लिए होने वाली औद्योगिक गतिविधियों में कमी लाएं। विकासशील देश कह रहे हैं कि वैश्विक जलवायु कार्यवाही के लिए ज्यादा वित्तीय साधनों की आवश्यकता है। हालांकि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन के लिहाज से देखें तो आज भी विकसित देशों की जलवायु परिवर्तन में हिस्सेदारी भारत जैसे देशों से कई गुना ज्यादा है।
जलवायु परिवर्तन से बढ़ रही गर्मी आजीविका, स्वास्थ्य, समाज के अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा बन रही है। महिलाएं इसकी भारी कीमत चुका रही हैं, गर्मी ने उनके दैनिक जीवन को काफी कठिन कर दिया है। आदिवासी, हिमालय के पर्वतीय भू-भाग में खेती के साथ-साथ जंगल से घास, लकड़ी और जलस्रोतों से पानी लाने के लिए महिलाओं पर एकतरफा जिम्मेदारी है। उनमें लगातार हो रही कमी के कारण महिला श्रमिकों के सिर और पीठ का बोझ बढ़ता जा रहा है और उन्हें तरह-तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। जरूरी है कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए बनायी जा रही नीतियों और योजनाओं को लैंगिक रूप से उत्तरदायी और संवेदनशील बनाया जाए।
‘विश्व मौसम विज्ञान संगठन’ (डब्ल्यूएमओ) ने भारत पर एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें जलवायु संकट के कारण 2011-20 के दशक को औसत से ज्यादा गर्मी और सर्वाधिक बारिश वाला बताया गया है। इस अवधि में जलवायु परिवर्तन की दर बढ़ी है। जो रिकॉर्ड में सबसे अधिक है। ‘संयुक्त राष्ट्र संघ’ द्वारा जलवायु,मौसम, जल-संसाधन पर किए गए शोध के मुताबिक उत्तर-पश्चिमी भारत, पाकिस्तान, चीन व अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी तट के लिए यह दशक सबसे अधिक गर्म रहा है।
ठंडे दिनों की संख्या लगातार घट रही है। पिछले दशक में 1961 से 1990 के दशकों की तुलना में ठंडे दिन 40 प्रतिशत घटे हैं। भारत में बाढ़ की समस्या भी बढ़ गई है। जून 2013 में भारी बारिश, पहाड़ों की बर्फ पिघलने की वजह से हिमालय क्षेत्र में बाढ़, भूस्खलन, भू-धंसाव की घटनाएं तेजी से बढ़ती जा रही हैं। बाढ़ के कारण इस दौरान भारत में हजारों मौतें हुई हैं। गर्मी आदि से बचने के लिए जीवन यापन पर बड़ा असर पड़ा है। आजीविका के सीमित साधनों के चलते लोगों की जेब पर भी बोझ बढ़ रहा है।
वर्ष 2022 तक की ‘आईपीसीसी’ (अंतरसरकार जलवायु परिवर्तन समिति) की रिपोर्ट के मुताबिक 1850 के स्तर से दुनिया का तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। अगर यह 1.7 से 1.8 डिग्री तक बढ़ता है तो दुनिया की आधी से अधिक आबादी का जीवन संकट में पड़ेगा। जलवायु नियंत्रण के लिए यदि कारगर उपाय नहीं हो सका तो इस सदी के अंत यानी 2100 तक धरती का तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है, जबकि जरूरी है कि धरती पर जीवन बचाने के लिए तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ोतरी न हो। जलवायु सम्मेलन हर साल हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि लोग अपने हिस्से के जलवायु संकट से निपटने के लिए वास्तविक कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इसका कारण है कि विकसित देशों ने प्रकृति का विनाश करके विकास के नाम पर जिस चकाचौंध को सामने लाए हैं उसी राह पर विकासशील देश भी चल रहे हैं। भोगवादी जीवन शैली और आधुनिक विकास के मॉडल से तो जलवायु संकट बढ़ने ही वाला है। (सप्रेस)
[block rendering halted]