73वें गणतंत्र दिवस पर विशेष
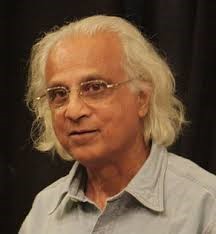
साल, हर साल नया होता है, लेकिन, जैसा मुक्तिबोध कहते हैं, ‘जो है, उससे बेहतर’ नहीं हो पाता। क्यों? क्या हमारे सोच और उसके अमल में ही कोई खोट है? या कि इसे कर पाने का हमारा वैचारिक ढांचा कमजोर है? अपनी बदहाली और उसके बदस्तूर जारी रहने को कैसे समझें और मुमकिन हो तो कैसे बदलें? हमारे 73वें ‘गणतंत्र दिवस’ पर इस बेहद जरूरी सवाल पर समाज-विज्ञानी दुनू राय का आलेख ।
साल 2021 समाप्त हुआ है। क्या इस समाप्ति में भविष्य की कोई झाँकी दिखती है?
पिछले वर्षों की तरह इस जनवरी 2022 में भी तीन प्रकार के नव-वर्षीय जश्न मनाए जा रहे हैं। पहला जश्न, उस संगठित वर्ग का है जो अपने शक्ति-प्रदर्शनकारी नेतृत्व की आराधना में लगा है: जिसने वायरस को परास्त किया; कश्मीर को आज़ाद किया; नागरिकता का नया परिचय दिया; चीनियों को मुहतोड़ जवाब दिया; भव्य राम मंदिर की स्थापना की; किसानों की कमाई को दुगुना किया; तथा राष्ट्रविरोधी, आन्दोलनजीवी और बगावती दलित, महिला, मुसलमान और अन्य ‘म्लेच्छों’ को ठिकाने लगा दिया।
दूसरा, बिखरा वर्ग तालाबंदी, नोटबंदी, गिरफ़्तारी और नफरती मुहीम के बावजूद इन सब कार्यकलापों के विरोध का, इंटरनेट के सहारे, आशावादी गुणगान कर रहा है। विद्यार्थी, मज़दूर, किसान, महिला, नर्स, डॉक्टर, शिक्षक, बेरोज़गार, वकील, इंजीनियर, बेघर, अपंग, व्यापारी, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुस्लमान, ईसाई और कुछ हिन्दू – सभी तबके, जहाँ हो सके, छोटे-बड़े समूहों में सड़क पर जुलूस भी निकाल रहे हैं।
और तीसरा जश्न, शोषक वर्ग मना रहा है, जो चुपचाप अपनी दौलत को एक-तिहाई बढ़ा चुका है, वो भी ऐसे समय में जब देश की दो-तिहाई जनता की कमाई घट गयी है। साथ में जनता को गुमराह करने के लिए कभी झूठे प्रचार, कभी नफरत और कभी डंडे और क़ैदख़ाने की नौटंकी लगातार चल रही है। इस तरह तीनों वर्ग अपने-अपने परिवर्तन का उत्सव मना रहे हैं, लेकिन क्या हैं, वो परिवर्तन?
शक्ति और शोषण की तरक्की का जश्न तो साफ़ समझ में आता है, लेकिन उनके विरोधियों के मन में परिवर्तन की कल्पना क्या है? कश्मीरी दो वर्ष बाद भी धारा-370 की बहाली की मांग कर रहे हैं। चीनियों से मुठभेड़ को उतावले उन्हें सीमा पार धकेलने पर अड़े हुए हैं। नागरिकता के सवाल पर सीएए (नागरिकता संशोधन अधिनियम) और एनआरसी (नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर) को रद्द करने के लिए कई गुट आज भी आमादा हैं। विद्यार्थी चाहते हैं कि पढ़ाई की फीस कम हो, नयी शिक्षा नीति को ख़त्म किया जाये, परीक्षाओं का सरलीकरण हो, विश्वविद्यालयों में दमन बंद हो और रोज़गार मिले।
तालाबंदी की स्थिति में प्रवासी मज़दूर को घर लौटने से डंडा भी रोक नहीं पाया था। और तो और, उनकी मदद के लिए एक जन समूह हर शहर, हर सड़क, हर वाहन पर तैनात हुआ। अब मांग रोज़गार गारंटी और सामाजिक सुरक्षा पर टिकी हुयी है।
चार नए श्रम कानूनों ने मज़दूर संगठनों को आम हड़ताल के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया। तीन कृषि कानूनों ने ऐतिहासिक किसान आंदोलन को जन्म दिया। बलात्कार, छेड़खानी, पितृसत्ता और लव-जिहाद के खिलाफ आवाज़ें तीव्र हुईं। अब “गोली मारो . . . को” जैसे नारों, उससे पैदा नरसंहार और गृह युद्ध की सम्भावना के सामने चुनौती देने वाले अपने-अपने मोर्चे पर डटे हुए हैं।
इन सभी आंदोलनों और प्रतिवादों में एक सूत्र दिखता है – कि समाज में प्रवाहित इन नयी प्रक्रियाओं को वापस लिया जाये; पुराने प्रजातंत्र को पुन: स्थापित किया जाये। वे पहले वर्ग के जश्न का विरोध तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से क्या वे भविष्य के किसी नए सपने को रख पा रहे हैं? अगर सभी नए कानूनों, नीतियों, चुनावी जुमलों और सामाजिक प्रचारों के लौटने की नौबत आती भी है तो क्या आतंक, तकरार, कु-शिक्षण, बेरोज़गारी, जातिवाद, पितृसत्ता, कृषि संकट इत्यादि के मूल कारण समाप्त हो जायेंगे ?
शायद हमें पचास साल पहले की वैचारिक बहस को फिर से टटोलने की ज़रूरत है, ताकि एक बेहतर समाज की कल्पना दुबारा सृजित हो सके। अगर हम आपसी वाद-विवाद के ज़रिये स्वीकार सकें कि वर्तमान की जाति, लिंग, धर्म और वर्ग आधारित दमन की राजनीति कहीं-न-कहीं एक आक्रामक (फासीवादी) पूंजीवादी व्यवस्था से जुडी है, तो शायद प्रतिरोध को भी केंद्र बिंदु मिल सकता है। आधुनिक पूंजीवाद की तीन मुख्य संचालक शक्तियां हैं – अधिक-से-अधिक मुनाफा कमाना; हमेशा श्रमजीवियों को चूसना; और प्रकृति को उन्मादी प्रवृत्ति से दोहना। गांधीजी के ताबीज़ (सबसे ग़रीब, सबसे असहाय की मुक्ति) के आधार पर क्या इन शक्तियों का मुक़ाबला किया जा सकता है?
इसमें कोई शक़ नहीं कि संविधान की रक्षा करना एक प्रशंसनीय कार्य है, लेकिन क्या वह एक भावी व्यापक दर्शन की तरफ ले जाता है? अगर ‘निवास’ की जगह ‘श्रम’ को नागरिकता का मूल आधार बनाना और ‘निर्देशक सिद्धांतों’ को बुनियादी अधिकारों के दायरे में लाना जैसी मांग उठाई जाएँ तो क्या वे हमारे संविधान को और जनपक्षीय नहीं बनाएंगे? गरीब के पास न ज़मीन है, न जन्मपत्री, लेकिन उसके पास मेहनत करने की क्षमता ज़रूर है और उसी मेहनत के बल पर राष्ट्र का निर्माण होता है। ‘निर्देशक सिद्धांत’ में ही आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक न्याय आखिरी व्यक्ति तक पहुँचाने की सम्भावना है, जिसमें समानता, आजीविका, आहार, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्व-शासन, सुरक्षा आदि सब कुछ शामिल हैं।
‘न्यूनतम वेतन’ और ‘न्यूनतम दाम’ की फुटकर मांग की जगह ‘जीवनोपयोगी कीमत’ (जिसमें पूरे परिवार की रोटी, कपड़ा, मकान सहित सभी आर्थिक और सामाजिक सुविधाएँ शामिल हैं और जिसे 1957 में ही त्रिपक्षीय – मज़दूर, मालिक और सरकार के बीच – मान्यता प्राप्त हुयी थी, और जिस पर 1991 में सर्वोच्च न्यायलय का ठप्पा भी लग गया था) के लिए संघर्ष से क्या पूँजी के खिलाफ श्रम की लड़ाई बुलंद नहीं हो जाएगी? और साथ में मज़दूर के पारिश्रमिक की लूट से बढते मुनाफे की कल्पना को भी घातक चोट नहीं पहुंचेगी? इस आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लूट को कैसे रोका जाये, यही एक ज्वलंत सवाल है।
इसी सवाल के जवाब से किसान और खेतिहर मज़दूर के बीच मज़बूत कड़ी बन सकती है जिससे वो अपने श्रम-आधारित हक़ को सशक्त करने के साथ खेती के आर्थिक और प्राकृतिक संकट का भी व्यावहारिक सामना कर सकते हैं। यह समझना ज़रूरी है कि ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य’ (एमएसपी) अगर ‘न्यूनतम वेतन’ पर आधारित होता है तो किसान और मज़दूर को उनके श्रम के बदले केवल 20 फीसदी हिस्सा ही मिलेगा; लेकिन अगर ‘जीवनोपयोगी वेतन’ के आधार पर ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य’ का आंकलन किया जाता है तो मूल्य तीन गुना (जो लगभग खुले बाज़ार के दाम के बराबर है) बढ़ने के साथ उसमें श्रम का 70 फीसदी हिस्सा भी शामिल हो जाएगा। अगर रासायनिक खेती की जगह पारम्परिक खेती की जाती है तो स्थानीय फसलों का उत्पादन बरक़रार रखते हुए उनका खर्च घटेगा और रोज़गार के अवसर बढेंगे।
इसी प्रकार केवल ‘असुरक्षित रोज़गार’ को बचाने की कोशिश के बजाय, संगठित मज़दूर ‘स्वस्थ और स्थायी जीविका’ की मांग के साथ मालिकों को चुनौती दे सकते हैं। निश्चित रोज़गार के अभाव में खतरनाक काम को कम पैसों में करने की मजबूरी मज़दूर की होती है, खासतौर से ऐसी स्थिति में जहाँ काम कम होता जा रहा है और बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। यह स्थिति सरकार की पूँजी के प्रति उदारवादी नीतियों की वजह से पैदा हुई है जिसमें पर्यावरणीय और जन-कल्याणकारी नियमों में ढिलाई साफ दिखती है। अगर जीवनोपयोगी वेतन का संगठित संघर्ष हुआ, जिससे दुर्घटनाग्रस्त या बेरोज़गार मज़दूर का भत्ता भी करीब तीन गुना बढ़ा, तो मज़दूर आंदोलन किसी भी राजनैतिक दल या सरकार पर सुरक्षित काम सम्बन्धी जन-परोपकारी नीति लाने के लिए प्रभावशाली राजनैतिक दबाव भी डाल सकते हैं।
अंत में, नफरत और भेदभाव की राजनीति की बात आती है – उसका क्या करें? जो सत्ता उस घृणा को प्रसारित कर रही है, क्या वो याचिकाओं और निवेदनों और अदालती हुक्मों से बाज़ आएगी? या उसकी जड़ को पहचानना ज़रूरी है? वो जड़ जो समाज कल्याण के नाम से पोषित हो रही है। ऐसे गिरोह से मुक्ति पाने के लिए एक इन्सानी परिवार की आवश्यकता है, जो सामूहिक काम और धाम को जोड़कर पारस्परिक सद्भावना और प्रेम के रिश्ते बनाये। अर्थात साथ मिलकर मेहनत करना, साथ मिलकर रहना, साथ मिलकर अपना भरण-पोषण करना, साथ मिलकर नीति बनाना, साथ मिलकर अपना शासन खुद करना: यही साम्यवादी विचार पूंजीवादी शोषण और साम-दाम-दंड-भेद की कूटनीति का उत्तर है।
रवींद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था, “प्रेम ने विश्व से कहा, मैं तुम्हारा हूँ; विश्व ने कहा, यह घर तुम्हारा है।” (सप्रेस)
[block rendering halted]



























