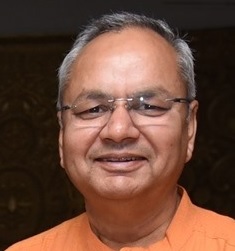
दूसरे विश्वयुद्ध के करीब सात दशक बाद का यह दौर दुनिया के आर्थिक ताने-बाने के लिहाज से वैसे भी खासा बदहवास था और ऐसे में दुनिया की पूंजी को हिलाने-डुलाने वाले अमरीका की गद्दी पर डोनॉल्ड ट्रम्प काबिज हो गए। अपनी बेहूदी, क्रूर और आत्मकेन्द्रित आर्थिक नीतियों के साथ ट्रम्प ने दुनियाभर में उथल-पुथल मचा दी है। ऐसे में भारत इस परिस्थिति से कैसे निपटे?
कभी राजनीति को समाजसेवा का माध्यम माना जाता था। पिछली सदी में महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन जैसी विभूतियों ने नैतिक मूल्यों पर आधारित राजनीति के जरिये सामाजिक बदलाव का कार्य किया, लेकिन अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करने के साथ ही राजनीति की दिशा में अप्रत्याशित परिवर्तन देखने को मिला। जनकल्याण और मानवता की सेवा का माध्यम मानी जाने वाली राजनीति, अब व्यवसायिक हितों को साधने का उपकरण बनती दिखने लगी है ।
डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के तुरंत बाद कई देशों के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। जॉर्डन, इज़राइल, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत और यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष उनसे मिलने ‘व्हाइट हाउस’ पहुंचे। इन बैठकों का केंद्र बिंदु ट्रम्प का प्रसिद्ध नारा ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ और उनकी टैरिफ नीतियों की सख्त धमकियां रहीं। अधिकांश नेताओं ने ट्रम्प की नीतियों पर शांतिपूर्वक संवाद किया, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत ने अप्रत्याशित रूप ले लिया। ट्रम्प, उनके उपराष्ट्रपति वेंस और ज़ेलेंस्की के बीच जिस तरह की तीखी बहस हुई, वैसी हालिया इतिहास में दुर्लभ है। इस तनावपूर्ण वार्ता ने न केवल कूटनीतिक हलकों में हलचल मचा दी, बल्कि वैश्विक राजनीति में भी नए समीकरणों के संकेत दिए।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दशकों तक एक-दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंद्वी रहे रूस और अमेरिका के बीच नजदीकियां बढ़ती दिख रही हैं। वहीं, अनुमान के विपरीत, राष्ट्रपति ट्रम्प का चीन के प्रति रवैया भी उतना सख्त नजर नहीं आ रहा। ग्रेट ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के सदस्य देश अमेरिका से धीरे-धीरे दूरी बनाते दिखाई दे रहे हैं। ‘गाजा पट्टी’ से फिलिस्तीनियों को हटाए जाने की आशंका से ग्रस्त मध्य-पूर्व के देशों में भी ट्रम्प प्रशासन के प्रति नाराजगी बढ़ रही है।
ट्रम्प की टैरिफ नीतियों से न केवल अंतरराष्ट्रीय संबंधों, बल्कि वैश्विक व्यापार पर भी व्यापक प्रभाव पड सकता है। ऐसे में दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक और तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था भारत के लिए भी यह परिदृश्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपनी भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक विविधता और आर्थिक क्षमता के कारण भारत हमेशा से वैश्विक मंच पर एक प्रभावशाली भूमिका निभाता रहा है। बदलते वैश्विक समीकरण भारत के कूटनीतिक और आर्थिक हितों को सीधे प्रभावित करेंगे, जिससे नई नीतियों और रणनीतियों की आवश्यकता बढ़ जाएगी।
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत की नीति संतुलन, बहुपक्षीय सहयोग और आत्मनिर्भरता पर आधारित रही है। वैश्विक व्यापार के संदर्भ में भारत अपनी उपस्थिति लगातार मजबूत कर रहा है, जहां निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है और आयात भी रणनीतिक आवश्यकताओं के अनुसार जारी है। हालांकि, व्यापार घाटे में असंतुलन एक महत्वपूर्ण चुनौती बना हुआ है। ऐसे में, अमेरिका के द्वारा प्रस्तावित ‘पारस्परिक टैरिफ’ का भारत की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है, जिससे व्यापार संतुलन और आर्थिक वृद्धि पर दबाव बढ़ सकता है। इससे निपटने के लिए भारत ने कूटनीतिक प्रयास तेज कर दिए हैं।
भारत ने ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते, द्विपक्षीय निवेश संधि और अलग सामाजिक सुरक्षा समझौते को लेकर व्यापार वार्ताएं दोबारा शुरू की हैं। जहाँ ब्रिटेन ने भारत से कार, व्हिस्की और अन्य वस्तुओं पर शुल्क में कमी का अनुरोध किया है, वहीं भारत ने ब्रिटेन में अपने सेवा क्षेत्र के पेशेवरों के लिए अधिक अवसर और आसान बाजार पहुंच की मांग रखी है।
प्रधानमंत्री मोदी और कतर के अमीर के बीच बातचीत ने दोनों देशों के मध्य व्यापार, ऊर्जा और निवेश में आपसी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। कतर, इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला मध्यस्थ और प्रमुख खिलाड़ी है। भारत में प्राकृतिक गैस की खपत में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है, जिससे आने वाले पांच वर्षों में भारत के ‘तरलीकृत प्राकृतिक गैस’ (एलएनजी) आयात में तेज़ी से वृद्धि होने की उम्मीद है।
भारत और ‘यूरोपीय संघ’ के बीच व्यापार और निवेश महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोनों पक्ष ने व्यापक ‘मुक्त व्यापार समझौते’ पर पुन: वार्ता शुरू की है। ‘यूरोपीय संघ’ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के नेतृत्व में ‘कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स’ के प्रतिनिधिमंडल की भारत यात्रा, भारत और यूरोप के बीच द्विपक्षीय संबंधों के एक नए महत्वपूर्ण चरण की शुरुआत को दर्शाती है। भारत और ‘यूरोपीय संघ’ के बीच व्यापार और निवेश, तकनीकी सहयोग, हरित ऊर्जा समाधान, जन-से-जन संपर्क, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में वार्ता जारी है। ‘यूरोपीय संघ’ में बढ़ता भारतीय प्रवासी समुदाय बड़ी संख्या में छात्रों, शोधकर्ताओं और कुशल पेशेवरों को शामिल करता है, जो दोनों पक्षों के संबंधों को और मजबूत बना रहा है।
व्यापारिक पहलों के साथ-साथ, भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने पर भी विशेष ध्यान देना होगा। भारत और चीन के संबंध ऐतिहासिक रूप से जटिल रहे हैं। व्यापार के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच व्यापक साझेदारी है, लेकिन सीमा विवाद और भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के चलते संबंधों में अक्सर तनाव भी देखने को मिलता है। भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह इस विवाद का समाधान कूटनीतिक संवाद और समझदारी भरी रणनीति के माध्यम से निकाले, ताकि क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक सहयोग को मजबूती मिल सके।
भारत के कुशल, लेकिन बेरोजगार पेशेवरों के लिए ‘यूरोपीय संघ’ में रोजगार के नए अवसर खुल सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि भारत अपने ‘कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों’ की गुणवत्ता में सुधार करे। साथ ही, भारतीय युवाओं को अंग्रेज़ी के अलावा एक या दो यूरोपीय भाषाएँ सिखाने के लिए विशेष संस्थान स्थापित किए जाएँ, जिससे उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़े।
भारत को ‘यूरोपीय संघ’ के साथ ‘कार्बन सीमा समायोजन तंत्र’ पर प्रभावी वार्ता कर कुछ रियायतें प्राप्त करनी होंगी। भारत इस्पात और एल्युमिनियम जैसे उत्पादों का प्रमुख निर्यातक है, लेकिन इन पर कार्बन टैक्स लगाए जाने से भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा, ‘यूरोपीय संघ’ भारतीय बाज़ार में कारों पर शुल्क रियायत की मांग कर रहा है। यह न केवल भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माताओं के लिए प्रतिकूल सिद्ध हो सकता है, बल्कि भारतीय सड़कों पर यूरोपीय कारों की संख्या में भी वृद्धि होगी, जिससे यातायात और सुरक्षा संबंधी नई चुनौतियाँ खड़ी हो सकती हैं। भारत को इस मांग को अत्यंत सावधानीपूर्वक और रणनीतिक रूप से संभालना होगा।
भारत ‘जी-20,’ ‘शंघाई सहयोग संगठन’ और ‘ब्रिक्स’ जैसे वैश्विक संगठनों में प्रभावी भागीदार है। अब समय आ गया है कि क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने भारत ‘दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन’ (सार्क) को पुनर्जीवित करने की दिशा में नेतृत्व करे। बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच, भारत को अपनी कूटनीतिक और आर्थिक नीतियों में संतुलन बनाए रखते हुए आगे बढ़ना होगा, ताकि वह अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में एक मजबूत, आत्मनिर्भर और प्रभावी भूमिका निभा सके। (सप्रेस)






























