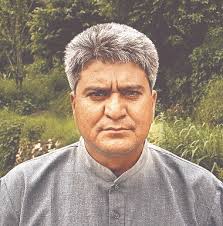
बड़ी,बारहमासी नदियों का दोहन करने की सरकारी हुलफुलाहट के साथ-साथ सत्तर के दशक से समाज ने भी इन पर गौर करना और जरूरी हो तो प्रतिरोध करना शुरु कर दिया है, लेकिन इन विशालकाय जल-भंडारों को पोषित करने वाली छोटी, स्थानीय नदियों की तरफ कौन देखता है? क्या इनकी बदहाली बड़ी नदियों को भी समाप्त नहीं कर देगी?
छोटी-छोटी नदियों से बनी गंगा 2550 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र और सिंधु क्रमशः 916 और 1114 किलोमीटर लंबी हैं। छोटी नदियां अनेक बड़ी नदियों के जल-बहाव को नियंत्रित करती हैं। लगभग सभी बड़ी नदियों के उद्गम ग्लेशियरों से हैं, लेकिन इनके निचले बहाव क्षेत्र में जंगल, तराई, मैदान और बीहड़ क्षेत्रों के बीच से छोटी-छोटी नदियां बड़ी नदियों में मिल रही हैं। छोटी नदियां पारिस्थितिकी तंत्र के कायाकल्प, जल और खाद्य सुरक्षा, आजीविका और समान सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
यमुना भारत की बड़ी नदी है जो इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। यमुना में भी टौंस, हिंडन, चंबल, बेतवा आदि मिलती हैं। रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, सोन आदि गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। चंबल और बेतवा उप सहायक हैं। पद्मा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश से निकलती हैं। चंबल में बनास, सिंध, बेतवा, केन मिलती हैं। सोन नदी में जोहिला, गोपद, रिहंद, कन्हार, उत्तरी कोयल मिलती हैं। नर्मदा में अमरावती, मुखी, तवा, बांगर मिलती हैं। गोदावरी में पैनगंगा, वर्धा, बनगंगा, इंद्रावती, साबरी, मंजीरा और कृष्णा में कोमना, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मुसी, मनेरू आदि मिलती हैं। कावेरी की सहायक नदियां हरंगी, हेमवती, काविनी, भवानी, अर्कावती, लक्ष्मणतीर्थं, नोट्याल आदि हैं।
छोटी नदियां भारत में बड़ी संख्या में हैं जो बड़ी नदियों के पोषक के रूप में मानी जाती हैं। छोटी नदियां बड़ी नदियों के प्रवाह को बढ़ाने के साथ-साथ भूजल पुनर्भरण को सक्षम बनाती हैं। मिट्टी की नमी, जैव-विविधता में सुधार करती हैं। सूखे और बाढ़ का सामना करने में मदद करती हैं, लेकिन देश में सूख रही छोटी नदियों का कायाकल्प समुदाय के बिना संभव नहीं है। गौरतलब है कि इन सहायक और छोटी-छोटी नदियों में निरंतर घटती जलराशि चिंता का विषय है। इसका कारण है कि इन नदियों के जल-ग्रहण क्षेत्र में वर्षों से जैव-विविधता का व्यवसायिक दोहन बड़े पैमाने पर हुआ है। खनन और अंधाधुंध भूजल का दोहन हो रहा है। मानवीय जीवन शैली ने नदियों को बेपानी बना दिया है। नदियों की जमीन और जलराशि में अतिक्रमण, शोषण, प्रदूषण के मौजूदा खतरे ने नदियों के पानी को स्नान लायक भी नहीं छोडा है।
ग्लेशियरों के सूखने से हिमपोषित नदियां भी सूख रही हैं। 45 डिग्री से भी अधिक तापमान के कारण छोटी नदियों का पानी लगभग सूख गया है। अप्रैल-जून की भीषण गर्मी से बुंदेलखंड की बहुत सारी नदियां सूख गई हैं जहां पानी के लिए हाहाकार है। पहाड़ी इलाकों में भी देखा जा सकता है जहां गंगा-जमुना की छोटी नदियां और जलस्रोत सूख गए हैं वहां भी लोग पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। ऐसे हालात पैदा होने के कुछ दिनों बाद होने वाली अनियमित और अनियंत्रित बारिश नदियों के जल-ग्रहण क्षेत्र में अपर्याप्त वनस्पतियों के अभाव में बाढ़ जैसी हालत पैदा करती हैं।
हर साल हिमालय से लेकर मैदानों तक भारी जल सैलाब से अपार जन-धन की हानि हो रही है। बारिश के पानी को रोकने की पारंपरिक शैली को आधुनिक विकास ने रौंद डाला है। जहां तालाब, जौहड जैसी जल संरचनाएं होती थीं, वहां सिंचाई और पेयजल के अलावा भूजल का भंडार भी पोषित होता था। अब उन स्थानों पर बहुमंजिली इमारतें, खनन, सीमेंटेड संरचनाओं ने पूरे जल क्षेत्र की जलवायु पर विपरीत प्रभाव डाल दिया है। भूजल बहुत नीचे चला गया।
इन चुनौतियों का सामना करते हुए आज भी भारत के हजारों गांवों में लोग अपने पारंपरिक प्रबंधन के अनुसार जल की व्यवस्था करते हैं जिससे स्वदेशी ज्ञान और प्रौद्योगिकी से विवेकपूर्ण जल उपयोग को बढ़ावा मिलता है। कुछ सक्रिय समाजसेवियों, पर्यावरणविदों और पानीदार समाज ने मिलकर ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जहां सूखी, छोटी नदियां फिर से बहने लगी हैं। यह तभी संभव हो पाया है जब स्थानीय समाज के साथ मिलकर नदियों के जल की पूर्व स्थिति और सूखने के कारणों की पड़ताल करके जल वापसी के उपाय पर संवाद हो सका है। कई स्थानों पर उदाहरण है कि लोगों ने सूखती छोटी नदियों के क्षेत्र का सामाजिक और पर्यावरणीय नक्शा तैयार करके एक पानीदार समाज का उदाहरण प्रस्तुत किया है।
अलवर में ‘तरुण भारत संघ’ एक उदाहरण है जिन्होंने सूखी नदियों को जिंदा कर दिया है। लोग वहां जाकर नदियों के पुनर्जीवन के सामाजिक और पर्यावरणीय तरीके सीख रहे हैं। बुंदेलखंड में ‘परमार्थ समाजसेवी संस्थान’ ने छोटी नदियों के पुनर्जीवन के लिए जोरदार अभियान चला रखा है। उन्होंने अब तक विलुप्त होती बछेड़ी नदी, कनेरा नदी, बरगी नदी, खूडर नदी, घुरारी नदी के पुनर्जीवन के लिए स्थानीय राज-समाज के साथ मिलकर महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं जो काफी सफल होते दिखाई दे रहे हैं। यहां का समाज अपनी नदियों को बचाने के लिए जागरूक है।
इस सीख को आगे बढ़ाने के लिए मध्यप्रदेश के खजुराहो में ‘जल जन जोड़ो अभियान’ और ‘परमार्थ समाजसेवी संस्थान’ द्वारा आयोजित एक संवाद में 15 राज्यों से आए 50 नदियों के प्रतिनिधियों ने निर्णय लिया कि 51 नदियों के पुनर्जीवन हेतु यात्रा का आयोजन किया जाएगा। पानी के काम में लगे राजेंद्र सिंह की अगुवाई में देश भर के जल विशेषज्ञों ने मांग की कि केन्द्र सरकार नदियों के लिए एक स्पष्ट ‘नदी नीति’ बनाये जिसकी मांग लंबे समय से उठाई जा रही है। नदियों पर काम करने वाले सभी लोग यह मानते हैं कि छोटी नदियों के जीवित रहने से समुदाय की खाद्य सुरक्षा, उनका सम्मानजनक जीवन और उनके आर्थिक विकास का संरक्षण होता है। इसके साथ ही वे बड़ी नदियों के प्रवाह को बढ़ाने, भूजल का पुनर्भरण करने, जमीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने में भी मददगार होती हैं।
जलवायु परिवर्तन का सीधा संबंध छोटी नदियों से है। यदि हम छोटी नदियों को जीवित कर लेंगे तो जलवायु परिवर्तन का खतरा कम हो जायेगा, लेकिन छोटी नदियों के पुनर्जीवन का काम समुदाय की अगुवाई के बिना संभव नहीं है। इस अभियान के राष्ट्रीय संयोजक संजय सिंह ने कहा कि नदियों को पुनर्जीवित करने हेतु निकाली जाने वाली यात्राओं के पहले यह जरूरी है कि संबंधित नदी के बारे में सारे आंकड़े एकत्रित करने के बाद समुदाय के साथ मिलकर संवाद किया जाए। प्रोफेसर विभूति राय कहते हैं कि 20 वर्षों में नदियां सूख जायेंगी। यदि पारंपरिक जल सुरक्षा के उपाय पर ध्यान नहीं दिया गया तो मानव जीवन पर संकट बढ़ जायेगा। नदियों के रिचार्ज का जब तक कोई सामान्य समाधान नहीं होगा तो नदियों को बचाना कठिन होगा।
देश के जल विशेषज्ञों की चिंता है कि जल संरक्षण हो या नदी पुनर्जीवन, सभी पर सरकारें पूरे देश के लिए एक जैसी योजना बनाती हैं। इसलिए यह काम धरातल पर नहीं दिखाई देता। यदि छोटी नदियों को पुनर्जीवित करना है तो हर क्षेत्र की जलवायु के अनुसार अलग-अलग नियोजन की आवश्यकता है। सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कटल कहते हैं कि नदियों को बचाने की आपातकालीन स्थिति है। इसलिए देशभर में नदियों के पुनर्जीवन के लिए चिंतित समाज और पर्यावरणविद् आगे आकर अपनी एक-एक नदी को पुनर्जीवित करने लिए कदम बढ़ाएं। (सप्रेस)































